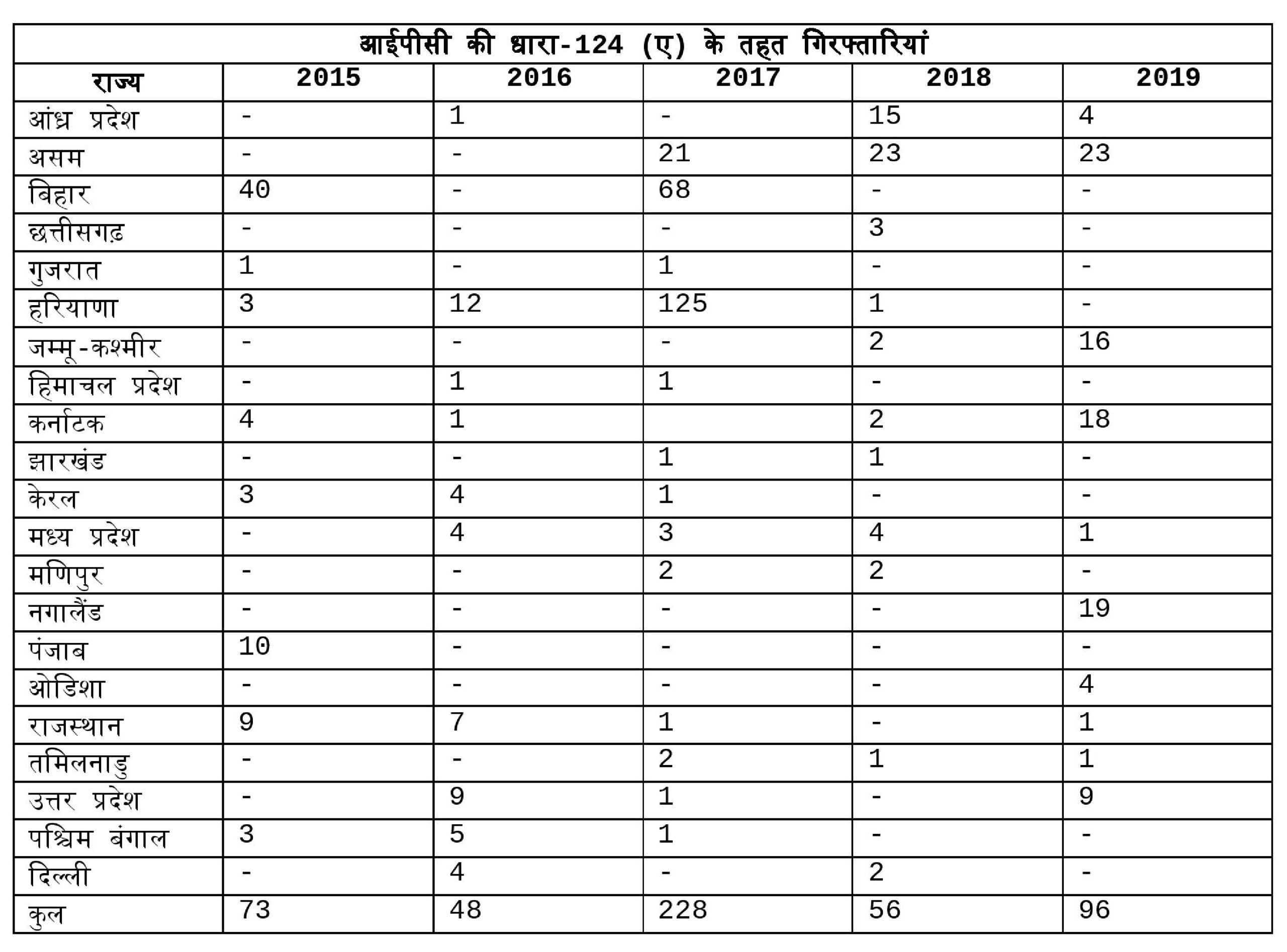संसद के नए भवन के शिलान्यास से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के व्यवहार को लेकर सख्त टिप्पणी की है. हालांकि, 10 दिसंबर को प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर पांच नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी के सवालों को उठाया गया था. इसके बावजूद सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ इमारतों को गिराने और पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया था.
‘हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप…’
सर्वोच्च अदालत का फैसला आए बगैर काम शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. अंग्रेजी वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ए.एम. खानविल्कर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘(प्रोजेक्ट पर) कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाई गई, इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम शुरू कर सकते हैं. हमने कोई आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि हमने माना कि आप (केंद्र सरकार) समझदार और विवेकपूर्ण वादी हैं और आप अदालत के प्रति सम्मान दिखाएंगे. हमने कभी नहीं सोचा था कि आप निर्माण कार्य के साथ इतनी आक्रामकता से आगे बढ़ जाएंगे. अभी ऐसी बहुत सी चीजें खुले तौर पर मौजूद हैं जो बताती हैं कि आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. हम नहीं ध्यान देते अगर आप सिर्फ पेपरवर्क या शिलान्यास करते. लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए.’ इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ शिलान्यास होगा, बाकी जमीन पर कोई तोड़फोड या निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल
प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है. इसके जरिए संसद के नए भवन के अलावा केंद्रीय सचिवालय की तीस इमारतों का निर्माण किया जाना है. हालांकि, कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के बीच इतनी खर्चीली प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने पर केंद्र सरकार को कई सवालों से जूझना पड़ रहा है. विपक्ष इसे महामारी जैसे हालात में सरकार की गलत प्राथमिकता बता रहा है. वहीं, सोशल मीडिया व दूसरे मंचों पर समाज के जागरुक नागरिक भी पूछ रहे हैं कि क्या इस महामारी के वक्त में सरकार के लिए संसद की नई इमारत ही सबसे जरूरी काम है?
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार की दलील
हालांकि, इन तमाम सवालों के बीच सरकार की अपनी दलील है. इसमें संसद भवन का लगभग 100 साल पुराना होना और जगह की कमी दो प्रमुख मुद्दा है. मौजूदा संसद भवन निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और 1927 को पूरा हुआ. इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें संसदीय कामकाज के लिए जगह की कमी है और आने वाले समय में यह जरूरत को पूरी नहीं कर पाएगा. खास तौर पर लोक सभा सीटों के परिसीमन के बाद जब सदस्यों की संख्य बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. इसके अलावा संसद में सदस्यों के अलग से बैठने के लिए जगह नहीं है. इसके अलावा जो नए निर्माण हुए हैं, वह भी जगह की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
ऑफिस के लिए जगह की कमी
केंद्र सरकार की यह भी दलील है कि अभी केंद्रीय सचिवालय 47 इमारतों में फैला है. इनमें से 30 इमारतें सेंट्रल विस्टा में आती हैं. लेकिन इनमें कामकाज से लेकर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह की भारी कमी है. इसके अलावा इन इमारतों की देखभाल, मरम्मत का खर्च भी बहुत ज्यादा है. संपत्ति विभाग के मुताबिक सेंट्रल विस्टा में ऑफिस के लिए 3.8 लाख वर्ग मीटर जगह की कमी है, जिससे किराए पर ऑफिस लेने से केंद्र सरकार का खर्च बहुत बढ़ जाता है. सरकार का कहना कि इससे विभागों और मंत्रालयों के अलग-अलग होने से कामकाज में तालमेल करने में भी समस्या आती है.
कहां कितने पुराने संसद भवन का इस्तेमाल
केंद्र सरकार की इन तमाम दलीलों के बीच सवाल वही है कि देश के सामने प्राथमिकता क्या है? दुनिया के तमाम देश, यहां तक कि विकसित देश संसद के पुराने भवनों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं. डच पार्लियामेंट अभी भी 13वीं सदी में बनी इमारत में चलती है. वहीं, इटली की संसद 16वीं सदी और फ्रांस की संसद 17वीं सदी की बनी इमारतों में चलती है. अन्य उदाहरणों को देखें तो अमेरिका की संसद वर्ष 1800 में बन कर पूरी हुई, जबकि ब्रिटिश संसद 1840 और 1870 के बीच बनी इमारतों में चल रही है. सवाल वही है कि क्या भारत में मौजूदा संसद भवन में बदलाव करके इसे भविष्य की जरूरत के लिए नहीं तैयार किया जा सकता है? अगर ऐसा करना बिल्कुल ही असंभव है तो क्या इस महामारी के वक्त में नए भवन के निर्माण को प्राथमिकता देना सही होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं, जहां लोगों को नुकसान न उठाना पड़ा हो या उन्हें सरकार से मदद की जरूरत न हो. सवाल तो यह भी है कि जो सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा करने की अपील कर रही हो, वह नई इमारतें बनाने पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च करना चाहती है?
ये भी पढ़ें– संसद की नई इमारत में क्या-क्या होगा?